आलेख
अजय बोकिल
तमिलनाडु की डीएमके सरकार और केन्द्र की मोदी सरकार के बीच जारी ‘भाषा युद्ध’ के तीसरे चरण में तमिलनाडु ने भारतीय मुद्रा रूपए का राष्ट्रीय चिन्ह बदलकर उसे तमिल वर्णमाला के अक्षर ‘र’ (रूपाई) में बदल दिया है। इसके पहले केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके के हिंदी विरोध को राजनीतिक बताते हुए कहा था कि राज्य सरकार पहले वहां तमिल भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो व्यवस्था करे। शाह के इस आदेशात्मक ‘सुझाव’ से यह बहस फिर तेज हो गई है कि क्या देश में अंग्रेजी के विकल्प के रूप में हिंदी व भारतीय भाषाअों में तकनीकी शिक्षा संभव है, अगर है तो कैसे? हालांकि मप्र जैसे राज्य ने ढाई साल पहले मेडिकल की पाठ्यपुस्तकें हिंदी में प्रकाशित करने की अच्छी पहल की थी। कुछ अन्य भारतीय भाषाअों में भी इसकी शुरूआत हुई है, लेकिन यहां प्रश्न स्व-भाषा अभिमान और मातृ भाषा में सुगम शिक्षा से कहीं ज्यादा जटिल और व्यावहारिक चुनौतियों से भरा है। यह काफी हद तक सम्प्रेषण की एकरूपता से जुडा है एवं ग्लोबल भी है। दरअसल स्थानीय भाषाअोंमें तकनीकी शिक्षा का भविष्य उन छात्रों के भविष्य से तय होगा, जो इस माध्यम में पढ़कर निकले हैं। यह शिक्षा उन छात्रों के पेशेवर ज्ञान की अद्यतनता, प्रामाणिकता, कॅरियर और आजीविका से कितनी जुड़ पाती है तथा तकनीकी एवं प्रौदयोगिकी क्षेत्र उनका कितना स्वीकार करते हैं, इस पर काफी कुछ निर्भर है। हकीकत में ऐसे नवाचारों को विद्यार्थियों के स्तर पर भी खास प्रतिसाद नहीं मिल पाया है। हिंदी में क्षेत्रीय भाषाअोंमें तकनीकी पुस्तकों की बहुत कमी है। जो अनुवाद हुए हैं, उनकी प्रामाणिकता तथा छात्रों की उनमें रूचि भी अहम है। ऐसी पुस्तकों को लेकर प्रकाशकों का रवैया भी बहुत उत्साहजनक नहीं है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार तमिलनाडु में भी कुछ शिक्षा संस्थानों में तमिल में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई है, लेकिन उसका प्रतिसाद लगभग वैसा ही है कि जैसे मप्र में हिंदी में इन विषयों की पढ़ाई को लेकर है। अव्वल तो बहुत ही गिने चुने विद्यार्थी ही हिंदी या अन्य भारतीय भाषा को इन विषयों की पढ़ाई का माध्यम चुनते हैं, क्योंकि उनके लिए इस संदर्भ में स्वभाषा प्रेम से ज्यादा रोजगार की चिंता होती है। वर्तमान में देश के लगभग सभी मेडिकल व इंजीनियरिंग काॅलेजो में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होती है। ऐसे में उनका आपसी संवाद भी बना रहता है। दूसरी तरफ हिंदी या क्षेत्रीय भाषा माध्यम से पढ़कर आने वाले विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी में विषय को समझना और आत्मसात करना कठिन होता है। उन्हें अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी होती है। कई बार मानसिक तनाव और न्यून ग्रंथि का शिकार भी होना पड़ता है।
हिंदी या मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा पाने वाले बच्चो के सामने महाप्रश्न यह है कि डिग्री लेने के बाद उनका भविष्य क्या है? कौन उन्हें नौकरी देगा? क्या सरकारें ऐसे स्नातकों को आरक्षण देंगी? दो अलग-अलग भाषा माध्यमों से शिक्षित डाॅक्टरों और इंजीनियरों में आपसी तालमेल कैसे बैठेगा? हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में पढ़े डाॅक्टर, इंजीनियरों को कहीं तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से दोयम तो नहीं मान लिया जाएगा? अगर नौकरी मिल भी गई तो इन विषयों में वैश्विक स्तर पर हो रहे शोध और अद्यतन ज्ञान उन्हें अपनी भाषा में कैसे, कब और कितना मिलेगा? यहां तक कि हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में उनकी मार्क शीट भी कितने लोग समझेंगे? यूं भी कारपोरेट में हिंदी या भारतीय भाषाअो के लिए कोई जगह नहीं है।

तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी और उससे सम्बद्ध कुछ काॅलेजों तथा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग काॅलेज तिरूनेलवेली में मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल में होने की जानकारी है। राज्य सरकार भी तमिल में पढ़े इंजीनियरों में से 20 फीसदी को नौकरी में प्राथमिकता देती है। लेकिन वहां भी तमिल में इंजीनियरिंग पढ़ने को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई देता, क्योंकि निजी कंपनियां ऐसे इंजीनियरों को नौकरी देने को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं रहतीं। उन्हें ऐसे छात्रों के इंजीनियरिंग ज्ञान के परफेक्शन पर संदेह रहता है। उधर विद्यार्थियों को लगता है कि क्षेत्रीय भाषा का अभिमान अपनी जगह है, लेकिन भारत में रोजगार जगत में इसकी कोई खास वकत नहीं है। इसके अलावा तकनीकी शब्दावली का तमिल या अन्य क्षेत्रीय भाषा में ठीक से अनुवाद उपलब्ध न होना भी है। कुछेक मामलों में ही मेडिकल की पढ़ाई भी तमिल में करने की प्रायोगिक सुविधा है। । यही वजह है कि क्षेत्रीय भाषा माध्यम वाली सीटों पर अधिकांश छात्र प्रवेश नहीं लेते। यूपी, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि का अनुभव भी यही रहा है। एआईसीटीई का डाटा कहता है कि हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा माध्यम वाली इंजीनियरिंग की ज्यादातर सीटें खाली रहती हैं। वर्ष 2021-22 में ऐसी 80 फीसदी खाली रहीं तो 2022-23 यह आंकड़ा 53 फीसद रहा। देश में सरकारी गैर सरकारी काॅलेजों को मिलाकर इंजीनियरिंग की 25 लाख सीटें हैं। तीन साल पहले देश के 22 इंजीनियरिंग काॅलेजों ने कुल 2580 सीटें हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा में इंजी पढ़ने वाले छात्रों को आॅफर की थीं। मप्र की राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित मैनिट काॅलेज में 2023 में 150 छात्रों ने हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया था, लेकिन बाद में 27 छात्र ही शेष रहे।
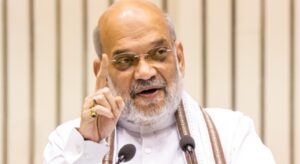
तो क्या अमित शाह का इशारा भी महज सियासी शगूफा ही है या फिर सरकार सचमुच भारतीय भाषाअों को तकनीकी ज्ञान का वाहक बनाने के लिए संकल्पित है? यह सही है कि जो बच्चे स्कूल स्तर पर हिंदी या अपनी मातृभाषा में पढ़कर मेडिकल और इंजीनियरिंग काॅलेजो में आते हैं, उन्हें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई में काफी दिक्कत आती है। कई बार तो वे समझ ही नहीं पाते। इसीलिए ये सोचा गया कि मेडिकल व इंजी. की किताबें भी हिंदी व अन्य भारतीय भाषाअों में तैयार की जाएं ताकि ग्रामीण परिवेश से आए विद्यार्थी विषय को आसानी से समझ सकें। मध्यप्रदेश में पहली बार अक्टूबर 2022 में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी माध्यम की किताबें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी की थीं। तर्क यही था कि जब रूसी,जापानी, जर्मन,चीनी आदि भाषाअोंमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो सकती है तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाअों में क्यों नहीं? क्यों हम अंग्रेजी पर ही निर्भर रहें। क्यों विदेशी भाषा का बोझ ढोते रहें?
दरअसल हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाअों में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेकर कई व्यावहारिक समस्याएं हैं। अभी ऐसे शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाई होती है। अगर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाअों में इन विषयों की पढाई होगी तो वो एक दूसरे से कैसे किस भाषा में संवाद करेंगे? मसलन तमिल माध्यम में पढ़ा छात्र उत्तर भारत के किसी डाॅक्टर या इंजीनियर के कैसे बात कर सकेगा? मलयालम में बनी डीपीआर हिंदी माध्यम वाला कैसे समझेगा? क्या इन क्षेत्रों में इतना जोखिम उठाया जा सकता है? यानी हमे हर स्तर पर अनुवाद और एकरूपता की जरूरत होगी और वह हमेशा प्रामाणिक ही हो, यह जरूरी नहीं है। दूसरे, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कितनी भाषाअों में शिक्षा दी जाएगी? उनका आपसी संपर्क किस भाषा में होगा। अगर वहां अंग्रेजी की जगह हिंदी विकल्प दिया गया तो दक्षिण व अन्य गैर हिंदी भाषी राज्य उन पर हिंदी थोपने का आरोप लगा सकते हैं, जो तमिलनाडु में हो ही रहा है, इससे और नई समस्या पैदा होंगी।

तमिल में शिक्षित मेडिकल प्रोफेसर उस राज्य के बाहर पढ़ाने की बात सोच भी नहीं सकता। हालांकि हिंदी वालों के लिए कुछ ज्यादा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम वालों ि जतने नहीं। दुनिया में इस विषयों से सम्बन्धित शोध पत्र अंग्रेजी में तुरंत अनूदित हो जाते हैं, लेकिन अन्य भाषााअों तक पहुंचने में बहुत समय लगता है या फिर वो हो ही नहीं पाते। हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा वाला विद्यार्थी डाॅक्टर अथवा इंजीनियर नए शोधों के बारे में जल्दी कैसे जानेगा? उसे उन शोध पत्रों का अनुवाद दूसरी भाषा में होने तक कितना इंतजार करना पड़ेगा? इससे भी बड़ी समस्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी संपर्क और संवाद की है। बेशक दुनिया में अंग्रेजी सबकी भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी डेढ़ अरब लोग इसे बोल या समझ सकते हैं।
वैसे यह सवाल पहले अंडा या मुर्गी की तरह है। हिंदी या क्षेत्रीय भाषाअों में तकनीकी विषय पढ़ाना शुरू ही नहीं करेंगे तो वो कभी भी नहीं होगा। इसका इलाज यही है कि आ रही दिक्कतों का समाधान ढ़ूंढा जाए लेकिन गुणवत्ता से किसी स्तर पर समझौता नहीं किया जाए। अनुवाद की कडि़यों को मजबूत किया जाए। उसे पूर्णत: विश्वसनीय और प्रामाणिक बनाया जाए। यह बहुत कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं बशर्ते कि वैसी संकल्पशक्ति और साफ नीयत हो।

-लेखक ‘सुबह सवेरे’ के कार्यकारी प्रधान संपादक हें।

